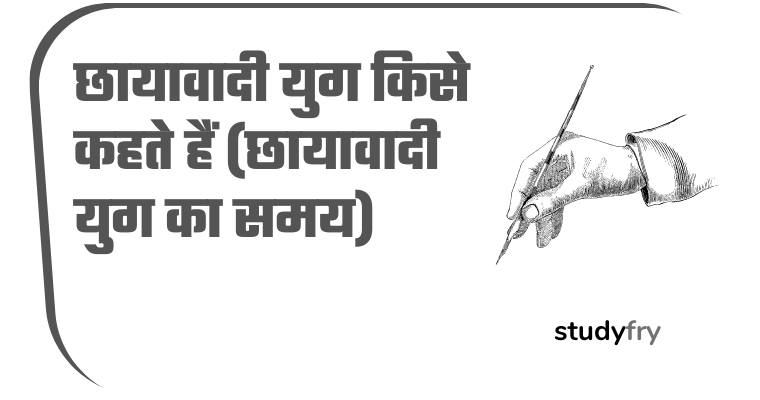छायावादी युग किसे कहते हैं (छायावादी युग का समय), छायावादी काव्य की विशेषताएँ (छायावादी युग की विशेषता), छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, छायावादी कवियों के नाम और उनकी रचनाएँ (छायावादी कवियों के नाम और उनकी रचनाएँ) आदि महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर यहाँ दिए गए हैं।
Table of Contents
छायावादी युग किसे कहते हैं (छायावादी युग का समय)
द्विवेदी युग के बाद के समय को छायावादी युग कहा जाता है। यह बीसवीं सदी का छायावादी कवियों के उत्थान का युग था। माना जाता है कि छायावादी युग का समय वर्ष 1920-1936 तक रहा। छायावादी युग में हिंदी साहित्य के क्षेत्र में भाव सरलता, गद्य गीत, मर्मस्पर्शी कल्पना, स्वतंत्र चिंतन आदि जैसे विचारों का समावेश है। छायावादी युग को प्रकृति एवं सौंदर्य पूजन कवियों का युग भी कहा जाता है। इस युग में महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी ‘निराला’, जयशंकर प्रसाद एवं सुमित्रानंदन पंत जैसे महान कवियों का उदय हुआ था। छायावादी युग में हिंदी कविता के स्वरूप में आंतरिक एवं बाहरी रूप से कई परिवर्तन आए थे। छायावादी युग में विशेष रूप से हिंदी काव्य के माध्यम से मानवीय क्रियाकलापों एवं भाव की प्रधानता को दर्शाया जाता है।
छायावादी काव्य की विशेषताएँ (छायावादी युग की विशेषता)
छायावादी काव्य में मुख्य रूप से व्यक्तिगत भावनाओं की प्रधानता होती है। छायावादी काव्य के माध्यम से एक कवि अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। छायावादी काव्य में नारी प्रेम, मानवीकरण, प्रकृति प्रेम, सौंदर्य कल्पना एवं सांस्कृतिक जागरण जैसे विचारों को अभिव्यक्त किया जाता है। इसके अलावा छायावादी काव्य की कई अन्य प्रमुख विशेषताएं भी हैं जो कुछ इस प्रकार हैं:-
- शृंगार भावना
- वेदना एवं करुणा की अधिकता
- सौंदर्य अनुभूति
- जीवन दर्शन
- नारी के प्रति नवीन भावना
- अज्ञात सत्ता के प्रति प्रेम भावना
- अभिव्यंजना शैली
- प्रकृति का मानवीकरण
शृंगार भावना
छायावादी काव्य में शृंगार भाव मुख्य रूप से विद्यमान होता है। इस काव्य में शृंगार को उपभोग की वस्तु ना मानकर उसे कौतूहल एवं विस्मय माना गया है।
वेदना एवं करुणा की अधिकता
छायावादी काव्य में वेदना एवं करुणा की भावना अधिक पाई जाती है। इसमें सौंदर्य की नश्वरता, प्रकृति की रहस्यमयता, अभिव्यक्ति की अपूर्णता, अभिलाषाओं की विफलता, प्रेयसी की निष्ठुरता आदि जैसे भाव को व्यक्त किया गया है।
सौंदर्य अनुभूति
छायावादी काव्य में सौंदर्य का तात्पर्य काव्य सौंदर्य से नहीं बल्कि सूक्ष्म आंतरिक सौंदर्य से होता है। यह बाहरी रूप से सौंदर्य की तुलना में आंतरिक सौंदर्य के भाव को दर्शाता है। छायावादी काव्य में कवियों ने नारी के सौंदर्य को कई प्रकार से व्यक्त करने का प्रयास किया है।
जीवन दर्शन
छायावादी काव्य में कवियों ने जीवन के मूल सिद्धांतों के दृष्टिकोण को अपनाया है। यह व्यक्ति के मूल दर्शन को सार्वजनिक रूप से दर्शाने का कार्य करता है। इसके अलावा छायावादी काव्य में संपूर्ण विश्व में पहली बार मानव चेतना को भी संपादित किया गया था।
नारी के प्रति नवीन भावना
छायावादी काव्य में यह दर्शाया गया है कि सौंदर्य एवं शृंगार का संबंध सीधे तौर पर नारी से होता है। इसमें नारी जाति को भाव जगत की सुकुमार देवी माना गया है।
अज्ञात सत्ता के प्रति प्रेम भावना
इस काव्य में मुख्य रूप से अज्ञात सत्ता के प्रति कवियों की हृदयगत प्रेम की भावना को व्यक्त किया गया है। इसमें कवि अज्ञात सत्ता को प्रेयसी या चेतन प्रकृति के रूप में देखते हैं। छायावाद काव्य की विशेषता यह है की इसमें यह अन्य सभी गुणों से भिन्न मानी जाती है।
अभिव्यंजना शैली
छायावादी काव्य में कवियों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने हेतु प्रतीकात्मक शैली एवं लाक्षणिक शैली को अपनाया है। इसमें कवियों ने लक्षण एवं व्यंजना का अधिक प्रयोग किया है।
प्रकृति का मानवीकरण
छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें प्रकृति को अनेक रूप में दर्शाया गया है। इसमें कवियों ने यह बताया कि वास्तव में प्रकृति पर मानव व्यक्तित्व का प्रभाव होता है। इसके अलावा छायावादी काव्य में प्रकृति को नारी का स्वरूप मानकर एक सूक्ष्म सौंदर्य का चित्रण किया गया है।
छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ
छायावाद की प्रमुख प्रवृतियाँ कुछ इस प्रकार हैं:-
- राष्ट्रीय/ सांस्कृतिक जागरण
- प्रकृति प्रेम
- आत्माभिव्यक्ति
- स्वच्छन्दतावाद
- कल्पना की प्रधानता
- रहस्यवाद
- दार्शनिकता
- शैलीगत प्रवृत्तियाँ
राष्ट्रीय/ सांस्कृतिक जागरण
छायावादी युग में कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से राष्ट्र एवं संस्कृति के प्रति प्रेम की भावना को व्यक्त किया है। इस युग में मुख्य रूप से मनुष्यों को देश प्रेम एवं संस्कृति के प्रति प्रेम की भावनाओं को उत्साहित करने वाली कविताएं लिखी गई हैं। केवल इतना ही नहीं इसमें कवियों ने देश के नागरिकों को जागृत करने हेतु भी कई कविताएं लिखी हैं।
प्रकृति प्रेम
छायावादी काव्य में मुख्य रूप से प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया है। छायावाद में कवियों ने प्रकृति के भीतर नारी के स्वरूप को उजागर किया है। इसमें मानव जीवन की समस्त भावनाओं एवं अनुभूतियों को प्रकृति के माध्यम से व्यक्त किया गया है। माना जाता है कि प्रकृति में नवीन चेतना को सर्वप्रथम छायावादी कवियों ने ही जागृत किया था।
आत्माभिव्यक्ति
छायावाद में मुख्य रूप से आत्माभिव्यक्ति की प्रधानता होती है। इसमें कवियों ने सामाजिक रूढ़ियों का अंत करने हेतु कई कविताओं की रचना की है। छायावाद में समस्त कवियों ने अपने कविताओं के माध्यम से आधुनिक युवा पीढ़ी को स्वयं को अभिव्यक्त करने हेतु सामाजिक स्वतंत्रता की आकांक्षा की है।
स्वच्छन्दतावाद
छायावादी युग में कवियों ने अपनी रचनाओं में प्रकृति का वर्णन एवं प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग किया है। यह दरअसल एक काव्य धारा है जो अंग्रेजी साहित्य के प्राकृतवाद (Romanticism) से प्रभावित है। वास्तव में कवि अपनी कविताओं को सामाजिक बंधनों से मुक्त कराना चाहते थे। स्वच्छंदतावाद कवियों के युगीन स्वतंत्र चेतना यानी मुक्ति के स्वर को दर्शाने का कार्य करता है।
कल्पना की प्रधानता
छायावाद में मुख्य रूप से मनोजगत (अंतर्जगत) की वाणी को उजागर करने का प्रयास किया गया है। इसमें व्यक्तिनिष्ठ एवं कल्पना के भाव की प्रधानता है। द्विवेदीयुगीन कविताओं में सृष्टि को व्यापक रूप से समेटने का कार्य किया गया है। इसके अलावा इसमें कवियों ने मनोजगत के सत्य को साकार करने हेतु ऊर्वरा कल्पनाशक्ति का प्रयोग किया है।
रहस्यवाद
रहस्यवाद वह भावनात्मक अभिव्यक्ति है जिसमें कोई कवि या रचनाकार अपनी रचनाओं के माध्यम से अपनी प्रेम भावना को उजागर करता है। छायावादी युग के महान कवियित्री महादेवी वर्मा जी की कविता में आध्यात्मिक प्रेम भावना का स्वरूप देखने को मिलता है।
दार्शनिकता
छायावाद में वेदांत से लेकर आनंदवाद तक का दार्शनिक प्रभाव देखने को मिलता है। इसमें मुख्य रूप से बौद्ध एवं महात्मा गांधी के विचारों का दर्शन भी देखा जा सकता है। इसमें धार्मिक एवं संस्कृति के क्षेत्रों में भी रूढ़िवाद की झलक देखी जा सकती है।
शैलीगत प्रवृत्तियाँ
छायावाद में प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद की शैलीगत प्रवृत्तियाँ देखी जा सकती हैं। जयशंकर प्रसाद ने अपनी रचनाओं के माध्यम से मार्मिकता में वृद्धि करने का कार्य किया है। उन्होंने अमूर्त को मूर्त एवं मूर्त को अमूर्त रूप में चित्रित करने हेतु कई रचनाएं की हैं।
छायावादी कवियों के नाम और उनकी रचनाएँ (छायावादी कवियों के नाम और उनकी रचनाएँ)
छायावादी युग में सूर्यकांत त्रिपाठी ‘निराला’, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा जी एवं सुमित्रानंदन पंत को काव्य के क्षेत्र का चार प्रमुख स्तंभ कहा जाता है। इसके अलावा माखनलाल चतुर्वेदी, हरिवंश राय बच्चन, रामकुमार वर्मा एवं रामधारी सिंह दिनकर को भी छायावादी कवियों के नाम से जाना जाता है।
छायावादी कवियों के नाम एवं उनकी प्रमुख रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं:-
सूर्यकांत त्रिपाठी ‘निराला’ (1898-1961 ई.)
सूर्यकांत त्रिपाठी ‘निराला’ की प्रमुख रचनाएं परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अनामिका, कुकुरमुत्ता, अणिमा, नए पत्ते, अर्चना, बेला आदि हैं।
जयशंकर प्रसाद (1889-1936 ई.)
जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं करुणालय, आंसू, कामायनी, लहर, महाराणा का महत्व, झरना, चित्र आधार (ब्रज भाषा में रचित कविता), कानन-कुसुम आदि है।
महादेवी वर्मा (1907-1988 ई.)
महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं निहार, नीरजा, दीपशिखा, यामा, रश्मि, सांध्यगीत आदि है।
सुमित्रानंदन पंत (1900-1977 ई.)
सुमित्रानंदन पंत की मुख्य रचनाएं प्रतिमा, शिल्पी, रजत-शिखर, वीणा, ग्रंथि, गुंजन, पल्लव, ग्राम्या, युगवाणी, स्वर्ण-धूलि, स्वर्ण-किरण, उत्तरा, युगांतर, अभिषेकित, लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद आदि है।
हरिकृष्ण ‘प्रेमी’ (1908 – 1974 ई.)
हरीकृष्ण प्रेमी की प्रमुख रचनाएं अनंत के पथ पर, रूप दर्शन, आंखों में, स्वर्णविहान, जादूगरनी, अग्निगान आदि है।
माखनलाल चतुर्वेदी (4 अप्रैल 1889 – 30 जनवरी 1968)
माखनलाल चतुर्वेदी की प्रमुख रचनाएं समर्पण, मरण ज्वार, हिमकिरीटिनी, युग चारण, माता, वेणु लो गूंजे धरा, बीजुरी काजल आँज, समय के पाँव, अमीर इरादे :गरीब इरादे, साहित्य के देवता, कृष्णार्जुन युद्ध आदि हैं।
हरिवंश राय बच्चन (27 नवम्बर 1907 – 18 जनवरी 2003)
हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचनाएं मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश, तेरा हार, बंगाल का काल, आत्म परिचय, एकांत संगीत, निशा निमंत्रण, सतरंगीनी, हलाहल, मिलन यामिनी, धार के इधर-उधर, खादी के फूल, जाल समेटा, त्रिभंगिमा, दो चट्टानें, आकुर अंतर, बहुत दिन बीते, आदि है।
रामधारी सिंह दिनकर (23 सितम्बर 1908- 24 अप्रैल 1974)
रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं बारदोली-विजय संदेश, रेणुका, रसवंती, हुंकार, धूप छांव, इतिहास के आंसू, नील कुसुम, सूरज का ब्याह, प्रिय कवि दिनकर, सीपी और शंख, आत्मा की आंखें, कोयला और कवित्य, रश्मिलोक, दिनकर की सूक्तियां आदि है।
डॉ रामकुमार वर्मा (15 सितम्बर, 1905 – 1990)
डॉ रामकुमार वर्मा की प्रमुख रचनाएं रूप राशि, अंजलि, चंद्रकिरण, चित्तौड़ की चिता, निशीथ, वीर हमीर, एकलव्य, अभिशाप आदि है।