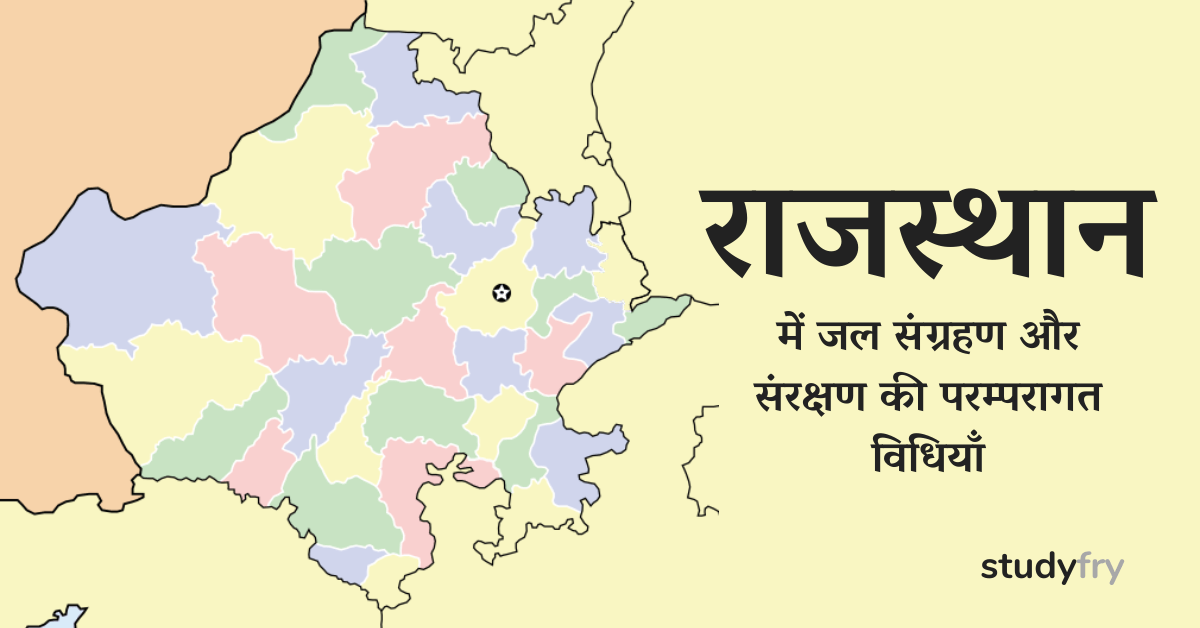राजस्थान में जल संग्रहण और संरक्षण की परम्परागत विधियाँ : राजस्थान में जल संग्रहण और जल के संरक्षण की कई सारी परम्परागत विधियाँ प्राचीनकाल से चली आ रही हैं। राजस्थान में जल संग्रहण और संरक्षण की कुछ विधियों में बावड़ी, नाड़ी, टाँका, जोहड़ और कुई आदि प्रमुख हैं।
Table of Contents
राजस्थान की प्राकृतिक जल-संग्रह तकनीकें
बावड़ी (Bawadi)
- बावड़ी (Stepwell) एक सीढ़ीदार बड़ा सा कुआँ होती है जिसमें भूमिगत जल और वर्षा का जल एकत्रित होता है।
- बावड़ीयों का निर्माण प्राचीनकाल से ही होता आ रहा है, कालिदास लिखित ‘मेघदूत’ में भी बावड़ी का उल्लेख मिलता है।
- राजस्थान स्थित कुछ प्रमुख बावड़ियों में ‘बूंदी की बावड़ी’ , दोसा स्थित ‘भाण्डरेज बावड़ी’ , चित्तोड़ स्थित ‘विनाता की बावड़ी’ और आभानेरी की ‘चाँद बावड़ी’ आदि हैं।

नाड़ी (Naadi)
- नाड़ी भूमि पर बनी एक गड्डानुमा आकृति होती है जिसमें वर्षा का जल एकत्रित होता है, यह एक तालाब जैसी आकृति होती है।
- नाड़ी को शेखावटी क्षेत्र में ‘नाड़ा’ के नाम से जाना जाता है।
- नाड़ी प्रमुखतः पश्चिमी राजस्थान में पायीं जाती हैं और अधिकांशतः जोधपुर में पायी जाती हैं।
- 1520 ई. में सर्वप्रथम नाड़ी का निर्माण मारवाड़ में जोधपुर के शासक राज जोधाजी ने करवाया था।
- नाड़ी की गहराई 5 से 12 मीटर तक होती है।
- नाड़ी में जिस रास्ते से पानी आता है उसे ‘आगौर’ कहा जाता है।
- नाड़ी से जल निकासी की उचित व्यवस्था की जाती है ताकि नाड़ी से अतिरिक्त जल पास स्थित दूसरी नाड़ी या खेत में चला जाये। जल निकासी के लिए बनाये गए इस रस्ते को ‘नेहटा’ कहा जाता है।
- नाड़ी में जल पहुँचाने के लिए निर्धारित की गयी भूमि को ‘मंदार’ कहा जाता है।
- नाड़ी का निर्माण ऐसी जगह किया जाता जहाँ ढलान से बहकर वर्षा का जल तालाब या नाड़ी में एकत्रित हो सके, साथ ही भूमि सघन या सख्त हो ताकि जल का रिसाव कम हो और जल लम्बे समय तक एकत्रित रहे।
- जिस ढालदार जमीन के क्षेत्र से वर्षा का जल आकर तालाब में इकट्ठा होता है उसे ‘आगोर या पायतन’ कहते हैं।

फोटो साभार – बेटर इंडिया
टोबा (Toba)
- टोबा जल संरक्षण एवं प्रबंधन की एक महत्वपूर्ण एवं पारम्परिक विधि है।
- टोबा का आकार भी नाड़ी के समान लेकिन बड़ा होता है। जिसमें वर्षा का जल साल भर एकत्रित रहता है।
- टोबा का निर्माण ऐसी भूमि में किया जाता है जोकि काफी सघन होती है और जिसमें से पानी का रिसाव कम होता है।
टाँका अथवा टाँके (Tanka / Tanke)
- राजस्थान में पीने का पानी एकत्रित करने के लिए जो भूमिगत टैंक अथवा कुंड का निर्माण किया जाता है उन्हीं को टाँका अथवा टाँके कहा जाता है।
- टाँका अथवा टाँके का आकार कमरे या कुएं जैसा बड़ा भी हो सकता है जोकि सामान्यतः ऊपर से ढका रहता है ताकि पीने का पानी लम्बे समय तक संरक्षित रखा जा सके।
- टाँका प्रमुखतः बीकानेर, फलोदी एवं बाड़मेर आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं।

जोहड़ (Johad)
- टाँका अथवा टाँके के समान ही वर्षा के जल को परम्परागत विधि द्वारा एक कुंड रूपी संरचना में संरक्षित किया जाता है जिसे राजस्थान राज्य के शेखावाटी क्षेत्र एवं हरियाणा राज्य में ‘जोहड़’ के नाम से जाना जाता है।
- जोहड़ का आकार गोलाकार होता है और टाँके से बड़ा होता है जोकि ऊपर से खुला होता है।
- जोहड़ में एकत्रित पानी का प्रयोग मनुष्य एवं पशुओं द्वारा पीने के लिए किया जाता है।

झालरा (Jhalra)
- अपने से ऊँचे तालाब एवं झील के रिसाव से प्राप्त पानी को संरक्षित करने के लिए झालरा का निर्माण किया जाता है।
- झालरा जल संचयन के एक महत्वपूर्ण विधि है जिसके जल का प्रयोग पेयजल के रूप में न करके धार्मिक रीति रिवाजों एवं सामूहिक स्नान आदि के लिए किया जाता था।
- झालरा का आकार आयताकार होता है जिसके तीन तरफ सीढियाँ बनी होती हैं।
तल्ली / पोखर (Talli / Pokhar)
- रेगिस्तान क्षेत्र में स्थित छोटे गड्डों में वर्षा के मीठे जल के भर जाने से तल्ली या पोखर का निर्माण होता है।
- तल्ली या पोखर का जल सूखने के बाद यह भूमि जिस उपजाऊ भूमि में बदल जाती है उसे ‘खड़ीन’ कहते हैं।
- खड़ीन का सर्वप्रथम प्रयोग जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मडों द्वारा 15 वीं. शताब्दी में किया गया था।
- जैसलमेर में लगभग 500 खड़ीन विकसित हैं जिनसे लगभग 1300 हैक्टेयर भूमि सिंचित की जाती है।
- खड़ीन का लगभग 5 से 7 किलो मीटर तक विस्तार होता है और इसकी पाल की ऊंचाई 2 से 3 मीटर तक होती है।
- खड़ीन का निर्माण इस तरीके से किया जाता है कि एक खड़ीन के भर जाने पर पानी दूसरे खड़ीन में चला जाये इसलिए खड़ीन ढलान वाली भूमि पर निर्मित होती है।
- खड़ीन की भूमि में नमी के आधार पर फसल उगाई जाती है।
- खड़ीन कृषि का प्रमुखतः प्रयोग जैसलमेर में किया जाता है।

फोटो साभार : flickr hindi water
कुई अथवा बेरी (Kui / Beri)
- कुई अथवा बेरी का निर्माण प्रमुखतः तालाब के पास किया जाता है ताकि तालाब का पानी रिस-रिस कर कुई अथवा बेरी में इकठ्ठा हो जाये।
- कुई अथवा बेरीयों का आकार सामान्यतः गोलाकार होता है जिसकी गहराई लगभग 10 से 12 मीटर तक होती है एवं इसके ऊपरी भाग को लकड़ी आदि की फंटियों द्वारा ढककर रखा जाता है ताकि पानी को अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सके।
- तालाब के सुख जाने पर भी कुई या बेरी में पानी उपलब्ध रहता है यही कारण है कि 1987 में पड़े भयंकर सूखे के बाद भी पीने का पानी उपलब्ध रहा।
- पश्चिमी राजस्थान एवं भारत और पाकिस्तान की सीमा से लगे क्षेत्रों में अधिकांशतः कुई अथवा बेरीयां पायी जाती हैं।
- बीकानेर एवं जैसलमेर आदि जिलों में कुई अथवा बेरी का अधिक प्रयोग किया जाता रहा है।
पढ़ें – राजस्थान का अपवाह तंत्र।
| क्लिक करें Rajasthan GK Notes पढ़ने के लिए |